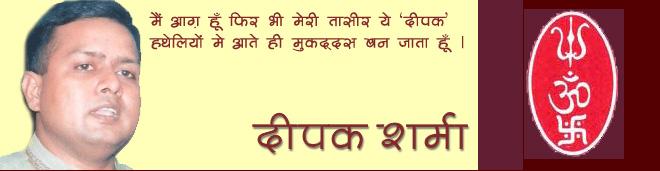मैं बिखर रहा हूँ मेरे दोस्त संभालो मुझको ,
मोतिओं से कहीं सागर की रेत न बन जाऊँ
कहीं यह ज़माना न उडा दे धूल की मानिंद
ठोकरें कर दें मजरूह और खून मे सन जाऊँ ।
इससे पहले कि दुनिया कर दे मुझे मुझ से जुदा
चले आओ जहाँ भी हो तुम्हे मोहब्बत का वास्ता
मैं बैचैनियो को बहलाकर कर रहा हूँ इन्तिज़ार
तन्हाइयां बेकरार निगाहों से देखती हैं रास्ता ।
बहुत शातिराना तरीके से लोग बात करते हैं ,
बेहद तल्ख़ अंदाज़ से ज़हान देता है आवाज़
मुझे अंजाम अपने मुस्तकबिल का नहीं मालूम
कफस मे बंद परिंदे कि भला क्या हो परवाज़ ।
अपनी हथेलियों से छूकर मेरी तपती पेशानी को
रेशम सी नमी दे दो , बसंत की फुहारे दे दो
प्यार से देख कर मुझको पुकार कर मेरा नाम
इस बीरान दुनिया मे फिर मदमस्त बहारें दे दो ।
आ जाओ इससे पहले कि चिराग बुझ जायें
दामन उम्मीद का कहीं ज़िन्दगी छोड़ न दे ,
सांस जो चलती हैं थाम कर हसरत का हाथ
"दीपक" का साथ कहीं रौशनी छोड़ ना दे ।
सर्वाधिकार सुरक्षित @कवि दीपक शर्मा
http://www.kavideepaksharma.co.in
http://shayardeepaksharma.blogspot.com
Saturday, April 25, 2009
Tuesday, April 7, 2009
मकान
जब से मेरे कान थोड़ा परिपक्व ही हुए थे
और मस्तिष्क शब्दों के रहस्य समझने लगा था ,
मुझे उस समय की हर बात अक्षरथः याद है ।
मुझे याद है , जब हमारा मकान बन रहा था
तो माँ से पिताजी ने बड़ी आत्मीयता से कहा था
कि ये मकान तुमारी धरोहर , मेरी स्मृति रहेगा
इसीलिए इतनी लगन से बनवा रहा हूँ ।
आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि
यह मकान मेरी वास्तव में पितृ - स्मृति है
और ये बात मुझसे ज्यादा शायद ये मकान भी जानता है ।
जब मैं छोटा था तो मकान कि ड्योढि़याँ
एक सुद्र्ढ़ युवा सीने सी तनी रहती थी
और मेरा निर्बाध आवागमन रहता था
शायद उन्हें खड़े रहने का पितृ - आदेश था ।
फ़िर जब मैं युवा हुआ तो मकान कि ड्योढि़याँ
युवावस्था कि सीमायें लाँघ चुकी थीं और
चल रहीं थीं संध्या के रवि कि तरह ।
फ़िर एक दिन मैं पितृ -स्मृति को अकेला छोड़
तरक्की के लिए गाँव से शहर कि और मुड गया
और अब एक अरसे बाद इसे बेचने आया हूँ
तो न चाहते हुए भी सोचने को विवश हो गया हूँ
कि जब धीरे - धीरे मेरे श्यामल केश
उम्र के साथ श्वेत परिधान पहन चुके हैं
तो ड्योढि़यों को भी घुन और दीमक ने
धीरे - धीरे पूर्णतया आलिन्गंबध कर लिया है ।
और जब मैं ड्योंढियों कि ओर देखता हूँ
तो मेरी नज़र ख़ुद - ब - ख़ुद झुक जाती है
मैं न जाने क्यों ड्योढियों नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ ।
" देखो हम तुम्हारी पितृ -स्मृति हैं "
हमने अपना हर कर्तव्य सत्यता से निभाया है
फ़िर हम तो तुम्हारे बचपन कि धरोहर हैं
तुम्हारे पिता कि स्नेह - स्मृति हैं ।
आदमी के साथ स्मृति जीवन तक रहती है
सो हम भी तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी ।
जब तुम दन्त विहीन हो जाओगे
तो हम भी कपाटहीन हो जायेंगी
और जब तुम्हारी कमर झुक जायेगी
तो हम भी स्वतः झुक जाएँगी
और जिस दिन हम गिरेंगी उस दिन तुम भी ..................... ।
बस बात अधूरी ही सोचकर मैंने दिमाग को झटका
शरीर कि फुरफुरी को मन से निकला
खड़े रोंगटे को हाथ से सहला , कान पे हाथ रखे
क्योंकि सत्यता सुनने का मनुष्य आदी नही होता ।
( उपरोक्त कविता कवि दीपक शर्मा जी के काव्य संकलन मंज़र से ली गई है )
सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा
और मस्तिष्क शब्दों के रहस्य समझने लगा था ,
मुझे उस समय की हर बात अक्षरथः याद है ।
मुझे याद है , जब हमारा मकान बन रहा था
तो माँ से पिताजी ने बड़ी आत्मीयता से कहा था
कि ये मकान तुमारी धरोहर , मेरी स्मृति रहेगा
इसीलिए इतनी लगन से बनवा रहा हूँ ।
आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि
यह मकान मेरी वास्तव में पितृ - स्मृति है
और ये बात मुझसे ज्यादा शायद ये मकान भी जानता है ।
जब मैं छोटा था तो मकान कि ड्योढि़याँ
एक सुद्र्ढ़ युवा सीने सी तनी रहती थी
और मेरा निर्बाध आवागमन रहता था
शायद उन्हें खड़े रहने का पितृ - आदेश था ।
फ़िर जब मैं युवा हुआ तो मकान कि ड्योढि़याँ
युवावस्था कि सीमायें लाँघ चुकी थीं और
चल रहीं थीं संध्या के रवि कि तरह ।
फ़िर एक दिन मैं पितृ -स्मृति को अकेला छोड़
तरक्की के लिए गाँव से शहर कि और मुड गया
और अब एक अरसे बाद इसे बेचने आया हूँ
तो न चाहते हुए भी सोचने को विवश हो गया हूँ
कि जब धीरे - धीरे मेरे श्यामल केश
उम्र के साथ श्वेत परिधान पहन चुके हैं
तो ड्योढि़यों को भी घुन और दीमक ने
धीरे - धीरे पूर्णतया आलिन्गंबध कर लिया है ।
और जब मैं ड्योंढियों कि ओर देखता हूँ
तो मेरी नज़र ख़ुद - ब - ख़ुद झुक जाती है
मैं न जाने क्यों ड्योढियों नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ ।
" देखो हम तुम्हारी पितृ -स्मृति हैं "
हमने अपना हर कर्तव्य सत्यता से निभाया है
फ़िर हम तो तुम्हारे बचपन कि धरोहर हैं
तुम्हारे पिता कि स्नेह - स्मृति हैं ।
आदमी के साथ स्मृति जीवन तक रहती है
सो हम भी तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी ।
जब तुम दन्त विहीन हो जाओगे
तो हम भी कपाटहीन हो जायेंगी
और जब तुम्हारी कमर झुक जायेगी
तो हम भी स्वतः झुक जाएँगी
और जिस दिन हम गिरेंगी उस दिन तुम भी ..................... ।
बस बात अधूरी ही सोचकर मैंने दिमाग को झटका
शरीर कि फुरफुरी को मन से निकला
खड़े रोंगटे को हाथ से सहला , कान पे हाथ रखे
क्योंकि सत्यता सुनने का मनुष्य आदी नही होता ।
( उपरोक्त कविता कवि दीपक शर्मा जी के काव्य संकलन मंज़र से ली गई है )
सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा
सागर के तट पर ...................
सागर के तट पर रेत के मैंने और तुमने
जो घरोंदें स्नेह के बनाये थे कभी
नयनों में अपनी कल्पनाओं के दीपक
साथ मिलकर जिस जगह जलाये थे कभी ।
अब वहां कुछ भी नज़र आता नहीं
बस टूटती लहरों के साये दीखते हैं ॥
कुछ पथिक , कुछ लहरों के क़दमों तले
स्वप्न सारे रेत हो रेत में मिल गये
रोंद कर घरोंदे निर्दयी पग के कारवां
काफिलों के रूप धर दूर निकल गये ।
गीत कोई मांझी अब वहां गाता नहीं
बस ह्रदय तड़पता है और अश्रु चीखते हैं ॥
अब नही वो अठखेलियाँ जिसकी फिजा में
आवाज मेरी आरजू की गूँजती थी
अब नही वहां लगते मेले चुहल के
ज़िन्दगी कल बेफिक्र जहाँ घुमती थी ।
अब पाँव लहरों में वहां कोई भिगोता नहीं
बस लहरें टकराती हैं और पत्थर भीगते हैं ।
दरख्त भी खामोश से उजड़े खड़े हैं
छाँव में जिनकी कभी बैठे थे हम तुम
घास जो चुभती थी बदन में मखमल सी
अब आँख बंद करके वहां खड़ी है गुमसुम
तिनका कोई तोड़ के मुंह में रखता नहीं
बस सीना उस जगह का पैर रौंदते हैं ।
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ति से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
जो घरोंदें स्नेह के बनाये थे कभी
नयनों में अपनी कल्पनाओं के दीपक
साथ मिलकर जिस जगह जलाये थे कभी ।
अब वहां कुछ भी नज़र आता नहीं
बस टूटती लहरों के साये दीखते हैं ॥
कुछ पथिक , कुछ लहरों के क़दमों तले
स्वप्न सारे रेत हो रेत में मिल गये
रोंद कर घरोंदे निर्दयी पग के कारवां
काफिलों के रूप धर दूर निकल गये ।
गीत कोई मांझी अब वहां गाता नहीं
बस ह्रदय तड़पता है और अश्रु चीखते हैं ॥
अब नही वो अठखेलियाँ जिसकी फिजा में
आवाज मेरी आरजू की गूँजती थी
अब नही वहां लगते मेले चुहल के
ज़िन्दगी कल बेफिक्र जहाँ घुमती थी ।
अब पाँव लहरों में वहां कोई भिगोता नहीं
बस लहरें टकराती हैं और पत्थर भीगते हैं ।
दरख्त भी खामोश से उजड़े खड़े हैं
छाँव में जिनकी कभी बैठे थे हम तुम
घास जो चुभती थी बदन में मखमल सी
अब आँख बंद करके वहां खड़ी है गुमसुम
तिनका कोई तोड़ के मुंह में रखता नहीं
बस सीना उस जगह का पैर रौंदते हैं ।
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ति से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
खून बेचने वाला
शहर के अस्पताल के बाहर, पेड़ की छांव तले
एक आदमी चुपचाप सूखी रोटी खा रहा था
उसके दाँत उस रोटी में गड़ नही रहे थे
पर भूख थी सो जबरन मुँह चला रहा था ।
बीच - बीच में अपनी बाँह से आँखे पोंछ लेता था
और कभी गौर से हाथों की लकीरें देख लेता था ।
मैं उसकी और लगातार देख रहा था
अचानक उसने भी मुझको देख लिया
क्यों भाई साहब, इस तरह से क्या देख रहे हो
थोड़ा घबराकर मुझसे उसने पूछ लिया ।
मैंने कहा - शायद तुम बहुत परेशान हो
तभी तो इतनी सूखी रोटी खा रहे हो
और खाते वक्त तो कोई भी नहीं रोता
मगर तुम हो कि रोते जा रहे हो ।
मेरी बात सुन कर वो फफक उठा
अन्दर ही अन्दर और तड़प उठा
थोड़ा संभल कर बोला - आप बजा फरमाते हैं
मैं थोड़ा नहीं , बेइन्तिहा परेशान हूँ
एक लाश हूँ, आदमी नहीं हूँ भाई साहब
खून की एक चलती फिरती दूकान हूँ ।
मैं अस्पतालों में अपना खून बेचता हूँ
तभी कहीं जाकर ये सूखी खा पाता हूँ
और इस धंधे से अपना ही नहीं
अपने परिवार का भी खर्चा चलता हूँ ।
और फ़िर खून बेचना भी आसान नहीं है
इसमें भी बहुत थपेड़े खाने पड़ते हैं
आधे डॉक्टर को और कुछ दलाल को
खून बेचने के लिए पैसे खिलने पड़ते हैं ।
अगर हम इन्हें पैसे न खिलाएं तो
रोग युक्त कहकर हमें डॉक्टर भगा देगा
गैर कानूनी खून बेचने के अपराध में
हो सकता है , कैद भी करवा देगा ।
उनका भी हिस्सा रहेगा पैसों में
इसी शर्त पर हम खून बेच पाते हैं
एक तरीके से इन लोगो को पैसा नहीं
ज़नाब हम अपना खून ही पिलाते हैं
तब कहीं जाकर ये रोटी मिल पाती है
या कहो - थोडी साँस और चल जाती है ।
उसकी बात सुनकर मैं अचरज से बोला
पड़े - लिक्खे लगते हो यार कुछ नौकरी कर लो
थोडी मेहनत करके और मजदूरी करके
ख़ुद का और परिवार का पेट भर लो ।
मुझ पर हँसते हुए फ़िर वो बोला
क्या नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती है ?
घूस यहाँ भी हजारों में खिलाई जाती है
और मैं पचास रुपये तो देख नहीं पाता
फ़िर ये हजारों रुपये कहाँ से लाऊंगा
अगर खून न बेचूं तो मेरे भाई
भूख से ही तड़प - तड़प के मर जाऊँगा
उसकी हर बात में सत्यता थी
इसलिए कुछ भी जवाब न दे पाया
पर एक बात , जेहन में , दिमाग में लेकर
चुपचाप वहां से मैं चला आया ।
राक्षस आदमी का लहू पीते हैं
ये सिर्फ़ आज तक किताबों में पड़ पाया था
मगर आज हकीकत में , इस दौर में
जिंदा राक्षसों से भी मिल आया था ।
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दिप्ति से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
एक आदमी चुपचाप सूखी रोटी खा रहा था
उसके दाँत उस रोटी में गड़ नही रहे थे
पर भूख थी सो जबरन मुँह चला रहा था ।
बीच - बीच में अपनी बाँह से आँखे पोंछ लेता था
और कभी गौर से हाथों की लकीरें देख लेता था ।
मैं उसकी और लगातार देख रहा था
अचानक उसने भी मुझको देख लिया
क्यों भाई साहब, इस तरह से क्या देख रहे हो
थोड़ा घबराकर मुझसे उसने पूछ लिया ।
मैंने कहा - शायद तुम बहुत परेशान हो
तभी तो इतनी सूखी रोटी खा रहे हो
और खाते वक्त तो कोई भी नहीं रोता
मगर तुम हो कि रोते जा रहे हो ।
मेरी बात सुन कर वो फफक उठा
अन्दर ही अन्दर और तड़प उठा
थोड़ा संभल कर बोला - आप बजा फरमाते हैं
मैं थोड़ा नहीं , बेइन्तिहा परेशान हूँ
एक लाश हूँ, आदमी नहीं हूँ भाई साहब
खून की एक चलती फिरती दूकान हूँ ।
मैं अस्पतालों में अपना खून बेचता हूँ
तभी कहीं जाकर ये सूखी खा पाता हूँ
और इस धंधे से अपना ही नहीं
अपने परिवार का भी खर्चा चलता हूँ ।
और फ़िर खून बेचना भी आसान नहीं है
इसमें भी बहुत थपेड़े खाने पड़ते हैं
आधे डॉक्टर को और कुछ दलाल को
खून बेचने के लिए पैसे खिलने पड़ते हैं ।
अगर हम इन्हें पैसे न खिलाएं तो
रोग युक्त कहकर हमें डॉक्टर भगा देगा
गैर कानूनी खून बेचने के अपराध में
हो सकता है , कैद भी करवा देगा ।
उनका भी हिस्सा रहेगा पैसों में
इसी शर्त पर हम खून बेच पाते हैं
एक तरीके से इन लोगो को पैसा नहीं
ज़नाब हम अपना खून ही पिलाते हैं
तब कहीं जाकर ये रोटी मिल पाती है
या कहो - थोडी साँस और चल जाती है ।
उसकी बात सुनकर मैं अचरज से बोला
पड़े - लिक्खे लगते हो यार कुछ नौकरी कर लो
थोडी मेहनत करके और मजदूरी करके
ख़ुद का और परिवार का पेट भर लो ।
मुझ पर हँसते हुए फ़िर वो बोला
क्या नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती है ?
घूस यहाँ भी हजारों में खिलाई जाती है
और मैं पचास रुपये तो देख नहीं पाता
फ़िर ये हजारों रुपये कहाँ से लाऊंगा
अगर खून न बेचूं तो मेरे भाई
भूख से ही तड़प - तड़प के मर जाऊँगा
उसकी हर बात में सत्यता थी
इसलिए कुछ भी जवाब न दे पाया
पर एक बात , जेहन में , दिमाग में लेकर
चुपचाप वहां से मैं चला आया ।
राक्षस आदमी का लहू पीते हैं
ये सिर्फ़ आज तक किताबों में पड़ पाया था
मगर आज हकीकत में , इस दौर में
जिंदा राक्षसों से भी मिल आया था ।
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दिप्ति से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
नहीं समय किसी का साथी रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
मत हँस इतना औरों पर कि
कल तुझको रोना पड़ जाये
छोड़ नर्म मखमली शैय्या को
गुदड़ पर सोना पड़ जाये
हर नीति यही बतलाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
तू इतना ऊँचा उड़ भी न कि
कल धरती के भी काबिल न रहे
इतना न समझ सबसे तू अलग
कल गिनती में भी शामिल न रहे
प्रीती सीख यही सिखलाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
रोतों को तू न और रुला
जलते को तू ना और जला
बेबस तन पर मत मार कभी
कंकड़ , पत्थर , व्यंग्यों का दल
अश्रु नहीं निकलते आँखों से
जीवन भर जाता आहों से
मन में छाले पड़ जाते हैं
अवसादों के विपदाओं से
कुदरत जब मार लगाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
इतना भी ऊँचा सिर न कर
औरों का कद बौना दिखे
इतनी भी ना कर नीचे नज़र
हर चीज़ तुझे नीची दिखे,
खण्ड - खण्ड अस्तित्व हो जाता है
पर लोक, ब्रह्माण्ड हो जाता है
साँसों कि हाट उजाड़ जाती
जब संयम प्रचंड हो जाता है
हर सदी यही दोहराती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
इतना मत इतर वैभव पर
अस्थिर धन के गौरव पर
पाण्डव का हश्र तुझे याद नहीं
ठोकर खायी थी पग - पग पर
मत हीन समझ औरों को तू
मत दीन समझ औरों को तू
मत हेय दृष्टि औरों पर डाल
मत वहम ग़लत ह्रदय में पाल
पल में पासा फ़िर जाता है
जब प्रकति नयन घुमती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
काया पर ऐसा गर्व ना कर
यौवन का इतना दंभ न भर
ना नाज़ कर इतना सुन्दरता पर
द्रग पर, केशों पर, अधरों पर
है नहीं ये कोई पूंजी ऐसी
जो आयु के संग बढती जाये
जैसे - जैसे चड़ती है उमर
ये वैसे - वैसे घटती जाये
अस्थि - अस्थि झुका साथी रे !
नहीं समय किसी साथी रे !
मत भाग्य किसी का छीन कभी
दाना हक़ से ज्यादा न बीन कभी
चलता रह अपनी परिधि में
पथ औरों का मत छीन कभी
वरना ऐसा भी तो हो जाता है
दाना अपना भी छिन जाता है
परिधि अपनी भी छुट जाता है
और भाग्य ही जड़ हो जाता है
जब एक दिन गगरी भर जाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
( उपरोक्त गीत कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दिप्ति से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
मत हँस इतना औरों पर कि
कल तुझको रोना पड़ जाये
छोड़ नर्म मखमली शैय्या को
गुदड़ पर सोना पड़ जाये
हर नीति यही बतलाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
तू इतना ऊँचा उड़ भी न कि
कल धरती के भी काबिल न रहे
इतना न समझ सबसे तू अलग
कल गिनती में भी शामिल न रहे
प्रीती सीख यही सिखलाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
रोतों को तू न और रुला
जलते को तू ना और जला
बेबस तन पर मत मार कभी
कंकड़ , पत्थर , व्यंग्यों का दल
अश्रु नहीं निकलते आँखों से
जीवन भर जाता आहों से
मन में छाले पड़ जाते हैं
अवसादों के विपदाओं से
कुदरत जब मार लगाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
इतना भी ऊँचा सिर न कर
औरों का कद बौना दिखे
इतनी भी ना कर नीचे नज़र
हर चीज़ तुझे नीची दिखे,
खण्ड - खण्ड अस्तित्व हो जाता है
पर लोक, ब्रह्माण्ड हो जाता है
साँसों कि हाट उजाड़ जाती
जब संयम प्रचंड हो जाता है
हर सदी यही दोहराती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
इतना मत इतर वैभव पर
अस्थिर धन के गौरव पर
पाण्डव का हश्र तुझे याद नहीं
ठोकर खायी थी पग - पग पर
मत हीन समझ औरों को तू
मत दीन समझ औरों को तू
मत हेय दृष्टि औरों पर डाल
मत वहम ग़लत ह्रदय में पाल
पल में पासा फ़िर जाता है
जब प्रकति नयन घुमती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
काया पर ऐसा गर्व ना कर
यौवन का इतना दंभ न भर
ना नाज़ कर इतना सुन्दरता पर
द्रग पर, केशों पर, अधरों पर
है नहीं ये कोई पूंजी ऐसी
जो आयु के संग बढती जाये
जैसे - जैसे चड़ती है उमर
ये वैसे - वैसे घटती जाये
अस्थि - अस्थि झुका साथी रे !
नहीं समय किसी साथी रे !
मत भाग्य किसी का छीन कभी
दाना हक़ से ज्यादा न बीन कभी
चलता रह अपनी परिधि में
पथ औरों का मत छीन कभी
वरना ऐसा भी तो हो जाता है
दाना अपना भी छिन जाता है
परिधि अपनी भी छुट जाता है
और भाग्य ही जड़ हो जाता है
जब एक दिन गगरी भर जाती रे !
नहीं समय किसी का साथी रे !
( उपरोक्त गीत कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दिप्ति से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
Monday, April 6, 2009
मैं भी चाहता हूँ
मैं भी चाहता हूँ की हुस्न पे ग़ज़लें लिक्खूं
मैं भी चाहता हूँ की इश्क के नगमें गाऊँ
अपने ख्वाबों में उतारूँ एक हसीन पैकर
सुख़न को अपने मरमरी लफ़्जों से सजाऊँ ।
लेकिन भूख़ के मारे, ज़र्द बेबस चेहरों पे
निगाह जाती है तो जोश काफू़र हो जाता है
हर तरफ हकीक़त में क्या तसव्वुर में
फ़कत रोटी का ही सवाल उभर कर आता है ।
ख़्याल आता है जे़हन में उन दरवाजों का
शर्म से जिनमें छिपे हैं जवान बदन कितने
जिनके तन को ढके हैं हाथ भर की कतरन
जिनके सीने में दफ़न हैं, अरमान कितने
जिनकी डोली नहीं उठी इस खातिर क्योंकि
उनके माँ -बाप ने शराफ़त की कमाई खाई है
चूल्हा एक बार ही जला हो घर में लेकिन
सिर्फ़ मेहनत की खाई है , मेहनत की खिलाई है ।
नज़र में घुमती है शक्ल उन मासूमों की
ज़िन्दगी जिनकी अँधेरा, निगाह समंदर है,
वीरान साँसे , पीप से भरी , धँसी आँखें
फाकों का पेट में चलता हुआ खंज़र है ।
माँ की छाती से चिपकने की उम्र है जिनकी
हाथ फैलाये वही राहों पे नज़र आते हैं ।
शोभित जिन हाथों में होनी थी कलमें
हाथ वही बोझ उठाते नज़र आते हैं ॥
राह में घूमते बेरोज़गार नौजवानों को
देखता हूँ तो कलेजा चीख़ उठता है
जिनके दम से कल रौशन ज़हान होना था
उन्हीं के सामने काला धुँआ सा उठता है ।
फ़िर कहो किस तरह हुस्न के नग्में गाऊँ
फ़िर कहो किस तरह इश्क पे ग़ज़लें लिक्खूं
फ़िर कहो किस तरह अपने सुखन में
मरमरी लफ़्जों के वास्ते जगह रखूं ॥
आज संसार में गम एक नही हज़ारों हैं
आदमी हर दुःख पे तो आंसूं बहा नही सकता ।
लेकिन सच है की भूखे होंठ हँसेंगे सिर्फ़ रोटी से
मीठे अल्फाज़ से कोई मन बहला नहीं सकता ॥
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ती से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
मैं भी चाहता हूँ की इश्क के नगमें गाऊँ
अपने ख्वाबों में उतारूँ एक हसीन पैकर
सुख़न को अपने मरमरी लफ़्जों से सजाऊँ ।
लेकिन भूख़ के मारे, ज़र्द बेबस चेहरों पे
निगाह जाती है तो जोश काफू़र हो जाता है
हर तरफ हकीक़त में क्या तसव्वुर में
फ़कत रोटी का ही सवाल उभर कर आता है ।
ख़्याल आता है जे़हन में उन दरवाजों का
शर्म से जिनमें छिपे हैं जवान बदन कितने
जिनके तन को ढके हैं हाथ भर की कतरन
जिनके सीने में दफ़न हैं, अरमान कितने
जिनकी डोली नहीं उठी इस खातिर क्योंकि
उनके माँ -बाप ने शराफ़त की कमाई खाई है
चूल्हा एक बार ही जला हो घर में लेकिन
सिर्फ़ मेहनत की खाई है , मेहनत की खिलाई है ।
नज़र में घुमती है शक्ल उन मासूमों की
ज़िन्दगी जिनकी अँधेरा, निगाह समंदर है,
वीरान साँसे , पीप से भरी , धँसी आँखें
फाकों का पेट में चलता हुआ खंज़र है ।
माँ की छाती से चिपकने की उम्र है जिनकी
हाथ फैलाये वही राहों पे नज़र आते हैं ।
शोभित जिन हाथों में होनी थी कलमें
हाथ वही बोझ उठाते नज़र आते हैं ॥
राह में घूमते बेरोज़गार नौजवानों को
देखता हूँ तो कलेजा चीख़ उठता है
जिनके दम से कल रौशन ज़हान होना था
उन्हीं के सामने काला धुँआ सा उठता है ।
फ़िर कहो किस तरह हुस्न के नग्में गाऊँ
फ़िर कहो किस तरह इश्क पे ग़ज़लें लिक्खूं
फ़िर कहो किस तरह अपने सुखन में
मरमरी लफ़्जों के वास्ते जगह रखूं ॥
आज संसार में गम एक नही हज़ारों हैं
आदमी हर दुःख पे तो आंसूं बहा नही सकता ।
लेकिन सच है की भूखे होंठ हँसेंगे सिर्फ़ रोटी से
मीठे अल्फाज़ से कोई मन बहला नहीं सकता ॥
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ती से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
यतीम
ये छोटे - छोटे से चेहरे
ये नाज़ुक तन, ये कोमल बदन
इन फूलों जैसे मासूमों के
सहमे - सहमे सकुचे बचपन ।
ये घोंट गला अरमानों का
ये तोड़ जिग़र आशाओं का
माँ के सानिध्य से बहुत दूर
ये हाथ पकड़ विपदाओं का
नयनों में लेकर शुष्क नीर
ह्रदय में शूल सी चुभती पीर
न सिर पे हाथ , न कोई साथ
ये बेदर, बेवज़ूद , ये बिन नीड़ ।
ये यतीम ये मासूम इतने ग़म कैसे पीते हैं
कितने ख़ामोश से रहते हैं , कितने ख़ामोश जीते हैं ॥
कोई इनको लावारिस कहता
कोई कहे औलाद नाजायज़ है
कोई कहे , खा लिये माँ - बाप
ये इसी सलूक के लायक हैं
कोई इनको गाली देता है
कोई इनको ताने देता है
कोई जान बूझ कर देता है
और कोई अनजाने देता है ।
लेकिन इसमें दोष कहाँ , इन मासूमों का, नादानों का
किस्मत लिखना काम नहीं, इंसानों की इंसानों का ॥
इनकी खातिर न सुबह हुई
न कोई रात, न कोई शाम
न धर्म पता, न कथा बंची
न रखा गया कोई भी नाम
गुदड़ तक नहीं इन लालों पर
तन पर भी नहीं पूरी कतरन
इन फूलों जैसे मासूमों के
सहमे - सहमे सकुचे बचपन
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ती से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
ये नाज़ुक तन, ये कोमल बदन
इन फूलों जैसे मासूमों के
सहमे - सहमे सकुचे बचपन ।
ये घोंट गला अरमानों का
ये तोड़ जिग़र आशाओं का
माँ के सानिध्य से बहुत दूर
ये हाथ पकड़ विपदाओं का
नयनों में लेकर शुष्क नीर
ह्रदय में शूल सी चुभती पीर
न सिर पे हाथ , न कोई साथ
ये बेदर, बेवज़ूद , ये बिन नीड़ ।
ये यतीम ये मासूम इतने ग़म कैसे पीते हैं
कितने ख़ामोश से रहते हैं , कितने ख़ामोश जीते हैं ॥
कोई इनको लावारिस कहता
कोई कहे औलाद नाजायज़ है
कोई कहे , खा लिये माँ - बाप
ये इसी सलूक के लायक हैं
कोई इनको गाली देता है
कोई इनको ताने देता है
कोई जान बूझ कर देता है
और कोई अनजाने देता है ।
लेकिन इसमें दोष कहाँ , इन मासूमों का, नादानों का
किस्मत लिखना काम नहीं, इंसानों की इंसानों का ॥
इनकी खातिर न सुबह हुई
न कोई रात, न कोई शाम
न धर्म पता, न कथा बंची
न रखा गया कोई भी नाम
गुदड़ तक नहीं इन लालों पर
तन पर भी नहीं पूरी कतरन
इन फूलों जैसे मासूमों के
सहमे - सहमे सकुचे बचपन
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ती से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
मयकश
लब तलक पैमाना लाने से पहले
याद कर मयकश अपने घर के मोहरे
फ़ाकों से टूटती बीवी की नफ़स
दाने - दाने को तरसते तेरे मोहरे ।
याद कर चीर में लिपटी हुई बीवी की शक़्ल
जिसने हाथों से उठाई है कै तेरी
तेरे हर ग़म पे गिराएँ हैं जिसने आँसूं
हँस के दामन में समेटी हैं तकलीफ़ें तेरी ।
तेरी बीमारी पे जिसने कड़कती रातें
न जाने कितनी दफ़ा आंखों में गुजारी होंगी ।
तेरी एक झूटी कराह पे भी जिसने
मन्नतें मांगी होंगी , नज़रें उतारी होंगी ॥
अरे ! मयक़्श तेरी श़ग्ले - मैजोशी ने
सोच क्या हालत तेरे घर की बना दी है,
तुझको और तेरे घर के हर श़ख्श को
एक रोटी भी ताज सा ख़्वाब बना दी है ।
मानता हूँ तेरा भी कोई ग़म होगा
लेकिन हर गम का मुदावा पैमाना तो नहीं
किसी ख्वाब के बिखर जाने का मतलब
ज़हर पीकर ज़िन्दगी मिटाना तो नहीं ।
सोच उन मासूमों का क्या मुस्तकबिल है
तेरी हर घूंट में शामिल है हक जिनका
गंदे ढेरों में तलाशते हैं जो ज़िन्दगी अपनी
एक टुकडा ही हसरत है, आरजू है जिनका ।
झाँककर देख एक बारगी उनकी निगाहों में
ज़िन्दगी किसी कोने में आंसू बहा रही होगी
घर के चूल्हे को जलते देखने की हसरत
कहीं बार - बार सिर अपना उठा रही होगी ।
इससे पहले कि तेरे होंठ जाम छू जायें
आगे बाद और तोड़ दे मय का प्याला
अरे मदहोश ! है प्याले के अन्दर अँधेरा
गौर से देख है बहार हँसता उजाला ।
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ती से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
याद कर मयकश अपने घर के मोहरे
फ़ाकों से टूटती बीवी की नफ़स
दाने - दाने को तरसते तेरे मोहरे ।
याद कर चीर में लिपटी हुई बीवी की शक़्ल
जिसने हाथों से उठाई है कै तेरी
तेरे हर ग़म पे गिराएँ हैं जिसने आँसूं
हँस के दामन में समेटी हैं तकलीफ़ें तेरी ।
तेरी बीमारी पे जिसने कड़कती रातें
न जाने कितनी दफ़ा आंखों में गुजारी होंगी ।
तेरी एक झूटी कराह पे भी जिसने
मन्नतें मांगी होंगी , नज़रें उतारी होंगी ॥
अरे ! मयक़्श तेरी श़ग्ले - मैजोशी ने
सोच क्या हालत तेरे घर की बना दी है,
तुझको और तेरे घर के हर श़ख्श को
एक रोटी भी ताज सा ख़्वाब बना दी है ।
मानता हूँ तेरा भी कोई ग़म होगा
लेकिन हर गम का मुदावा पैमाना तो नहीं
किसी ख्वाब के बिखर जाने का मतलब
ज़हर पीकर ज़िन्दगी मिटाना तो नहीं ।
सोच उन मासूमों का क्या मुस्तकबिल है
तेरी हर घूंट में शामिल है हक जिनका
गंदे ढेरों में तलाशते हैं जो ज़िन्दगी अपनी
एक टुकडा ही हसरत है, आरजू है जिनका ।
झाँककर देख एक बारगी उनकी निगाहों में
ज़िन्दगी किसी कोने में आंसू बहा रही होगी
घर के चूल्हे को जलते देखने की हसरत
कहीं बार - बार सिर अपना उठा रही होगी ।
इससे पहले कि तेरे होंठ जाम छू जायें
आगे बाद और तोड़ दे मय का प्याला
अरे मदहोश ! है प्याले के अन्दर अँधेरा
गौर से देख है बहार हँसता उजाला ।
( उपरोक्त नज़्म कवि दीपक शर्मा के काव्य संकलन फलक दीप्ती से ली गई है )
(सर्वाधिकार सुरक्षित @ कवि दीपक शर्मा )
nazm
मेरी सांसों में यही दहशत समाई रहती है
मज़हब से कौमें बँटी तो वतन का क्या होगा।
यूँ ही खिंचती रही दीवार ग़र दरम्यान दिल के
तो सोचो हश्र क्या कल घर के आँगन का होगा।
जिस जगह की बुनियाद बशर की लाश पर ठहरे
वो कुछ भी हो लेकिन ख़ुदा का घर नहीं होगा।
मज़हब के नाम पर कौ़में बनाने वालों सुन लो तुम
काम कोई दूसरा इससे ज़हाँ में बदतर नहीं होगा।
मज़हब के नाम पर दंगे, सियासत के हुक्म पे फितन
यूँ ही चलते रहे तो सोचो, ज़रा अमन का क्या होगा।
अहले-वतन शोलों के हाथों दामन न अपना दो
दामन रेशमी है "दीपक" फिर दामन का क्या होगा।
इस सन्देश को भारत के जन मानस तक पहुँचाने मे सहयोग दे.ताकि इस स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके औरआवाम चुनाव मे सोच कर मतदान करे.
काव्यधारा टीम
( सर्वाधिकार सुरक्षित @कवि दीपक शर्मा )
Subscribe to:
Posts (Atom)